
–संजय चावला-
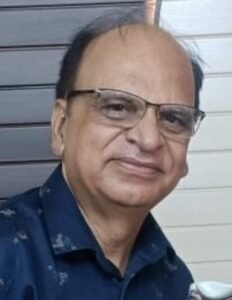
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने मई माह में एक ऐतिहासिक फैसला लिया है: सत्र 2025-26 से कक्षा 1 और 2 में मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाई अनिवार्य होगी। यह निर्णय नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और विभिन्न शिक्षा आयोगों की उस सिफारिश की पुष्टि करता है, जिसमें कहा गया है कि प्रारंभिक वर्षों में बच्चों को उन्हीं की मातृभाषा में पढ़ाना उनके संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास के लिए अत्यंत लाभकारी है। अनेक अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय शोधों से यह सिद्ध हो चुका है कि बच्चा सबसे पहले और सबसे गहराई से उसी भाषा को समझता और अपनाता है जिसे वह घर में सुनता और बोलता है। मातृभाषा न केवल उसके सीखने की गति को तेज़ करती है, बल्कि भावनात्मक जुड़ाव भी बढ़ाती है। इसके उलट, अपरिचित भाषा में दी गई शिक्षा अक्सर बच्चे को शिक्षा प्रणाली से काट देती है।
लेकिन सवाल है कि कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जैसे हाड़ौती क्षेत्र में जब इस नीति को लागू किया जाएगा, तब सीबीएसई से संबद्ध निजी स्कूल किस भाषा को ‘मातृभाषा’ मानेंगे? क्या वे वास्तव में स्थानीय बहुसंख्यक भाषा हाड़ौती को प्राथमिकता देंगे — या एक बार फिर हिंदी (खड़ी बोली) को “मातृभाषा” कहकर नीति की आत्मा को दरकिनार कर देंगे?
2011 की जनगणना के अनुसार कोटा संभाग में लगभग 48 प्रतिशत जनसंख्या की मातृभाषा हाड़ौती है। यह भाषा न केवल देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, बल्कि इसमें हिंदी से अलग उच्चारण और व्याकरणिक संरचना पाई जाती है। भाषाविदों के अनुसार हाड़ौती, हिंदी की एक उपबोली नहीं बल्कि एक स्वतंत्र भाषा है, जिसकी जड़ें हिंदी से भी पुरानी हैं। इसके बावजूद, कोटा के अधिकांश निजी स्कूल हाड़ौती को शैक्षणिक भाषा के रूप में स्वीकार करने से कतराएंगे। उनका बहाना पहले से तय है: “हमें न तो प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध हैं, न पाठ्यपुस्तकें और न ही शिक्षण-सामग्री।” असल में, यह बहाना एक गहरी मानसिकता को उजागर करता है — जिसमें भाषाई विविधता को भार माना जाता है, पूंजी और ब्रांडिंग को प्राथमिकता दी जाती है, और मातृभाषा को ‘गांव की भाषा’ समझकर उपेक्षित किया जाता है।
कोटा जैसे बहुसांस्कृतिक शहर में जहाँ तमिल, मलयालम, बांग्ला, पंजाबी और मराठी भाषी समुदाय भी रहते हैं, मातृभाषा आधारित शिक्षा के लिए एक बहुभाषीय ढांचा विकसित करना ज़रूरी है, ना कि सिर्फ हिंदी को थोप देना। मातृभाषा आधारित शिक्षा का मतलब यह नहीं कि सभी को एक ही भाषा पढ़ाई जाए, बल्कि इसका मतलब है — हर बच्चे को उसकी अपनी भाषा में सिखाया जाए।
आज हाड़ौती भाषा एक सांस्कृतिक अभिव्यक्ति है, एक स्थानीय पहचान है और एक शैक्षिक अवसर भी। यदि स्कूल चाहें तो स्थानीय विद्वानों, शिक्षकों और साहित्यकारों की मदद से एक प्रारंभिक पाठ्यक्रम विकसित किया जा सकता है। शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा सकता है। सबसे बड़ी बात — अभिभावकों को विश्वास में लिया जा सकता है। यह भी समझना ज़रूरी है कि मातृभाषा आधारित शिक्षा का मतलब अंग्रेज़ी या हिंदी से दूरी नहीं है। बच्चे हाड़ौती में बुनियादी शिक्षा लेकर हिंदी और अंग्रेज़ी में भी दक्ष बन सकते हैं — जड़ें अपनी, पंख सबके लिए।
अब समय आ गया है कि सीबीएसई स्कूल यह स्पष्ट करें कि वे इस नीति को केवल औपचारिकता के तौर पर निभाएंगे या वास्तव में हाड़ौती भाषा को कक्षा में सम्मान और स्थान देंगे। यदि आज हम हाड़ौती को शिक्षा का माध्यम नहीं बनाते, तो कल यह केवल घर की दीवारों तक सिमट जाएगी। अगर ईमानदारी से प्रयास हुआ तो वह दिन दूर नहीं जब हाड़ौती न केवल घरों की बोली, बल्कि विद्यालयों की भाषा भी बनेगी — और इससे जुड़ी पीढ़ियों की आत्मा और अस्मिता दोनों मजबूत होंगी।

















